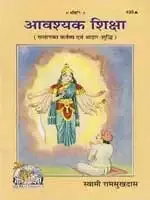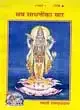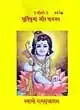|
गीता प्रेस, गोरखपुर >> आवश्यक शिक्षा आवश्यक शिक्षास्वामी रामसुखदास
|
392 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है आवश्यक शिक्षा....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
आवश्यक शिक्षा
मनुष्यमात्र वास्तव में विद्यार्थी ही है। देवता, यक्ष, राक्षस, पशु,
पक्षी आदि जितनी स्थावर-जंगम योनियाँ हैं, वे सब भोगयोनियाँ हैं। उनमें
मनुष्ययोनि केवल ब्रह्मविद्या प्राप्त करने के लिये है, अविद्या और भोग
प्राप्त करने के लिये नहीं।
मनुष्यशरीर केवल परमात्मप्राप्ति के लिये ही मिला है; अतः परमात्मप्राप्ति कर लेना ही वास्तव में मनुष्यता है। इसलिये मनुष्ययोनि वास्तव में साधनयोनि ही है। मनुष्य योनि में जो अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, यदि उनमें मनुष्य सुखी-दुःखी होता है तो वह भोगयोनि ही हुई और भोग भोगने के लिये वह नये कर्म करता है तो भी उसमें भोगयोनि की ही मुख्यता रही। अतः अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति को साधन-सामग्री बना लेना और भोग भोगने तथा स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से नये कर्म न करना, प्रत्युत परमात्मप्राप्ति के लिये शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्तव्यकर्म करना ही मनुष्यता है। इस दृष्टि से मनुष्य मात्र को साधक, विद्यार्थी कह सकते हैं।
मनुष्य-जीवन में आश्रमों के चार विभाग किये गये हैं—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जैसे, सौ वर्ष की आयु में पचीस वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम, पचीस से पचास वर्ष तक गृहस्थाश्रम, पचास से पचहत्तर वर्ष तक वानप्रस्थाश्रम और पचहत्तर से सौ वर्ष तक संन्यासाश्रम बताया गया है। ब्रह्मचर्याश्रम (विद्यार्थी-जीवन)—में गुरु-आज्ञाका पालन, गृहस्थाश्रम में अतिथि-सत्कार, वानप्रस्थाश्रम में तपस्या और संन्यासाश्रम में ब्रह्मचिन्तन करना मुख्य है।
ब्रह्मचारी (विद्यार्थी) दो तरह के होते हैं—नैष्ठिक और उपकुवार्ण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे होते हैं, जो अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, विवेक-विचार के द्वारा भोगाशक्ति का त्याग करके परमात्मा की तरफ चल पड़े हैं। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी वे होते हैं, जो विचार के द्वारा भोगासक्ति का त्याग नहीं कर सके; अतः केवल भोगाशक्ति को मिटाने के लिये गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश करते हैं। वे शास्त्रविधि पूर्वक विवाह करते हैं और धर्मका पालन करते हुए त्यागदृष्टि से उपार्जन और भोग करते हैं। उनके सामने धर्म की मुख्यता रहती है। धर्म का पालन करने से उनको भोग और संग्रह से स्वतः वैराग्य हो जाता है—‘धर्म तें बिरति’ (मानस 3/16/1) और वे परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं।
प्रश्न—विद्यार्थी किसे कहते हैं ?
उत्तर—जो केवल विद्याध्ययन करना चाहता है, उसको विद्यार्थी करते हैं। ‘विद्यार्थी’ शब्द का अर्थ है—विद्या का अर्थी अर्थात् केवल विद्या चाहने वाला। कौन-सी विद्या ? विद्याओं में श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या—‘अध्यात्मविद्या विद्यानाम्’ (गीता 10/32)
प्रश्न- विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है ?
उत्तर —कुछ भी जानना विद्या है। अनेक शास्त्रों का, कला-कौशलों का, भाषाओं आदि का ज्ञान विद्या है। वास्तव में विद्या वही है, जिससे जानना बाकी न रहे, जीवकी मुक्ति हो जाय—‘सा विद्या या विमुक्तये’ (विष्णुपुराण 1/19/41)। अगर जानना बाकी रह गया तो वह विद्या क्या हुई !
एक शब्दब्रह्म (वेद) है और एक परब्रह्म (परमात्मतत्त्व) है अगर शब्दब्रह्म को जान लिया, पर परब्रह्म को नहीं जाना तो केवल परिश्रम ही हुआ—
मनुष्यशरीर केवल परमात्मप्राप्ति के लिये ही मिला है; अतः परमात्मप्राप्ति कर लेना ही वास्तव में मनुष्यता है। इसलिये मनुष्ययोनि वास्तव में साधनयोनि ही है। मनुष्य योनि में जो अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, यदि उनमें मनुष्य सुखी-दुःखी होता है तो वह भोगयोनि ही हुई और भोग भोगने के लिये वह नये कर्म करता है तो भी उसमें भोगयोनि की ही मुख्यता रही। अतः अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति को साधन-सामग्री बना लेना और भोग भोगने तथा स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से नये कर्म न करना, प्रत्युत परमात्मप्राप्ति के लिये शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्तव्यकर्म करना ही मनुष्यता है। इस दृष्टि से मनुष्य मात्र को साधक, विद्यार्थी कह सकते हैं।
मनुष्य-जीवन में आश्रमों के चार विभाग किये गये हैं—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जैसे, सौ वर्ष की आयु में पचीस वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम, पचीस से पचास वर्ष तक गृहस्थाश्रम, पचास से पचहत्तर वर्ष तक वानप्रस्थाश्रम और पचहत्तर से सौ वर्ष तक संन्यासाश्रम बताया गया है। ब्रह्मचर्याश्रम (विद्यार्थी-जीवन)—में गुरु-आज्ञाका पालन, गृहस्थाश्रम में अतिथि-सत्कार, वानप्रस्थाश्रम में तपस्या और संन्यासाश्रम में ब्रह्मचिन्तन करना मुख्य है।
ब्रह्मचारी (विद्यार्थी) दो तरह के होते हैं—नैष्ठिक और उपकुवार्ण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे होते हैं, जो अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, विवेक-विचार के द्वारा भोगाशक्ति का त्याग करके परमात्मा की तरफ चल पड़े हैं। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी वे होते हैं, जो विचार के द्वारा भोगासक्ति का त्याग नहीं कर सके; अतः केवल भोगाशक्ति को मिटाने के लिये गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश करते हैं। वे शास्त्रविधि पूर्वक विवाह करते हैं और धर्मका पालन करते हुए त्यागदृष्टि से उपार्जन और भोग करते हैं। उनके सामने धर्म की मुख्यता रहती है। धर्म का पालन करने से उनको भोग और संग्रह से स्वतः वैराग्य हो जाता है—‘धर्म तें बिरति’ (मानस 3/16/1) और वे परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं।
प्रश्न—विद्यार्थी किसे कहते हैं ?
उत्तर—जो केवल विद्याध्ययन करना चाहता है, उसको विद्यार्थी करते हैं। ‘विद्यार्थी’ शब्द का अर्थ है—विद्या का अर्थी अर्थात् केवल विद्या चाहने वाला। कौन-सी विद्या ? विद्याओं में श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या—‘अध्यात्मविद्या विद्यानाम्’ (गीता 10/32)
प्रश्न- विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है ?
उत्तर —कुछ भी जानना विद्या है। अनेक शास्त्रों का, कला-कौशलों का, भाषाओं आदि का ज्ञान विद्या है। वास्तव में विद्या वही है, जिससे जानना बाकी न रहे, जीवकी मुक्ति हो जाय—‘सा विद्या या विमुक्तये’ (विष्णुपुराण 1/19/41)। अगर जानना बाकी रह गया तो वह विद्या क्या हुई !
एक शब्दब्रह्म (वेद) है और एक परब्रह्म (परमात्मतत्त्व) है अगर शब्दब्रह्म को जान लिया, पर परब्रह्म को नहीं जाना तो केवल परिश्रम ही हुआ—
शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि।
श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः।।
श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः।।
(श्रीमद्भा. 11/11/18)
अतः परमात्मतत्त्व को जानना ही मुख्य विद्या है और इसी में
मनुष्यजीवन की सफलता है।
जिससे जीविका का उपार्जन हो, नौकरी मिले, वह भी विद्या है, पर वह विद्या परमात्मप्राप्ति में सहायक नहीं होती, प्रत्युत कहीं-कहीं उस विद्या का अभिमान होने से वह विद्या परमात्मप्राप्ति में बाधक हो जाती है। विद्या के अभिमानी को कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिल जाय तो वह तर्क करके उनकी बात को काट देगा, उनको चुप करा देगा, जिससे वह वास्तविक लाभ से वञ्चित रह जायगा। अतः कहा गया है—
जिससे जीविका का उपार्जन हो, नौकरी मिले, वह भी विद्या है, पर वह विद्या परमात्मप्राप्ति में सहायक नहीं होती, प्रत्युत कहीं-कहीं उस विद्या का अभिमान होने से वह विद्या परमात्मप्राप्ति में बाधक हो जाती है। विद्या के अभिमानी को कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिल जाय तो वह तर्क करके उनकी बात को काट देगा, उनको चुप करा देगा, जिससे वह वास्तविक लाभ से वञ्चित रह जायगा। अतः कहा गया है—
षडंगदिवेदो मुखे शास्त्रविद्या
कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति।
यशोदाकिशोरे मनो वै न लग्नं
ततः किं ततः किं ततः किम् ततः किम्
कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति।
यशोदाकिशोरे मनो वै न लग्नं
ततः किं ततः किं ततः किम् ततः किम्
‘छहों अंगोंसहित वेद और शास्त्रों को पढ़ा हो, सुन्दर गद्य और
पद्ममय काव्य-रचना करता हो, पर यदि यशोदानन्दन में मन नहीं लगा तो उन सभी
से क्या लाभ है ?’
प्रश्न—विद्या ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है ?
उत्तर—विद्याके बिना मनुष्यजन्म सार्थक नहीं होगा, प्रत्युत मनुष्यजन्म और पशुजन्म एक समान ही होंगे। अतः विद्या की अत्यन्त आवश्यकता है।
कोई भी आरम्भ होता है तो वह किसी उद्देश्य को लेकर ही होता है। मनुष्यजन्म केवल दुःखों का अत्यन्ताभाव और परमानन्द की प्राप्ति के उद्देश्य से ही मिला है। इस उद्देश्य की सिद्धि अगर नहीं हुई तो मनुष्यता नहीं है। जैसे पशु-पक्षी आदि भोगयोनि है, ऐसे ही परमात्मप्राप्ति के बिना मनुष्य भी भोगयोनि ही है। कारण कि परमात्मप्राप्ति का अवसर प्राप्त करके भी मनुष्य केवल भोगों में लगा रहा तो वह भोगयोनि ही हुई। और उसका पतन ही हुआ— ‘तमारुढच्युतं विदुः’ (श्रीमद्भा. 11/7/74)।
यदि मनुष्य जन्म चौरासी लाख योनियों में जाने के लिये, बार-बार जन्मने-मरने के लिए ही हुआ तो फिर उसमें मनुष्यता क्या हुई ? अतः मनुष्य जन्म में विद्यार्थी को परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिये, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं—
प्रश्न—विद्या ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है ?
उत्तर—विद्याके बिना मनुष्यजन्म सार्थक नहीं होगा, प्रत्युत मनुष्यजन्म और पशुजन्म एक समान ही होंगे। अतः विद्या की अत्यन्त आवश्यकता है।
कोई भी आरम्भ होता है तो वह किसी उद्देश्य को लेकर ही होता है। मनुष्यजन्म केवल दुःखों का अत्यन्ताभाव और परमानन्द की प्राप्ति के उद्देश्य से ही मिला है। इस उद्देश्य की सिद्धि अगर नहीं हुई तो मनुष्यता नहीं है। जैसे पशु-पक्षी आदि भोगयोनि है, ऐसे ही परमात्मप्राप्ति के बिना मनुष्य भी भोगयोनि ही है। कारण कि परमात्मप्राप्ति का अवसर प्राप्त करके भी मनुष्य केवल भोगों में लगा रहा तो वह भोगयोनि ही हुई। और उसका पतन ही हुआ— ‘तमारुढच्युतं विदुः’ (श्रीमद्भा. 11/7/74)।
यदि मनुष्य जन्म चौरासी लाख योनियों में जाने के लिये, बार-बार जन्मने-मरने के लिए ही हुआ तो फिर उसमें मनुष्यता क्या हुई ? अतः मनुष्य जन्म में विद्यार्थी को परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिये, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं—
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।।
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।।
(गीता 6/22)
‘जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने
में भी
नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर मनुष्य बड़े भारी दुःख से भी विचलित
नहीं किया जा सकता।’
वास्तव में ब्रह्मविद्या ही विद्या है, अन्य विद्या तो अविद्या है। कारण कि ब्रह्मविद्या के प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य (लौकिक) विद्याएँ नहीं पढ़नी चाहिये। अन्य विद्याएँ भी पढ़नी चाहिये। अन्य भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान-सम्पादन करना उचित है, पर उनमें ही लिप्त रहना उचित नहीं है; क्योंकि उनमें ही लिप्त रहने से मनुष्य जन्म निरर्थक चला जायगा। दूसरी बात, लौकिक विद्याओं को पढ़ने से ‘मैं पढ़ा-लिखा हूँ’—ऐसा एक अभिमान पैदा हो जाएगा, जिससे बन्धन और दृढ़ हो जायगा।
वास्तव में ब्रह्मविद्या ही विद्या है, अन्य विद्या तो अविद्या है। कारण कि ब्रह्मविद्या के प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य (लौकिक) विद्याएँ नहीं पढ़नी चाहिये। अन्य विद्याएँ भी पढ़नी चाहिये। अन्य भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान-सम्पादन करना उचित है, पर उनमें ही लिप्त रहना उचित नहीं है; क्योंकि उनमें ही लिप्त रहने से मनुष्य जन्म निरर्थक चला जायगा। दूसरी बात, लौकिक विद्याओं को पढ़ने से ‘मैं पढ़ा-लिखा हूँ’—ऐसा एक अभिमान पैदा हो जाएगा, जिससे बन्धन और दृढ़ हो जायगा।
शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा
यस्तु क्रियावान्पुरुषः स विद्वान्।
यस्तु क्रियावान्पुरुषः स विद्वान्।
‘शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख बने रहते हैं। वास्तव में
विद्वान वही है, जो शास्त्र के अनुकूल आचरण करता है।’
मनुष्य जन्म का उद्देश्य है—परमात्मतत्त्व की प्राप्ति करना और उसका साधन है—संसार की सेवा। अतः लौकिक विद्या, धन, पद आदि का उपयोगी संसार की सेवा में ही है। ये संसार की सेवा में ही काम आ सकते हैं, परमात्मप्राप्ति में नहीं, क्योंकि परमात्मप्राप्ति लौकिक विद्या के अधीन नहीं है। जिसके पास लौकिक विद्या आदि है, उसी पर संसार की सेवा करने की जिम्मेवारी है। मालपर ही जकात लगती है और इन्कम पर ही टैक्स लगता है। माल नहीं है तो जकात कि बात की ? इन्कम नहीं तो टैक्स किस बात का ?
लौकिक विद्या, धन, पद आदि को लेकर संसार में मनुष्य की जो प्रशंसा होती है, वह एक तरह से मनुष्य की निन्दा ही है। तात्पर्य है कि महिमा तो लौकिक विद्या आदि की ही हुई, खुदकी तो निन्दा ही है। अतः जो लौकिक विद्या आदि से अपने को बड़ा मानता है, वह वास्तव में अपने को छोटा ही बनाता है।
प्रश्न—विद्याध्ययन बाल्यावस्थामें ही करना चाहिये या आजीवन ?
उत्तर—बाल्यावस्था में विद्याध्ययन करने का नियम केवल उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिये ही है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है,
उसको तो आजीवन शास्त्रों का, ब्रह्मविद्या का अध्ययन करते रहना चाहिये।
प्रश्न—अगर कोई विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हुए बीच में ही मर जाय तो उसकी क्या गति होगी ?
उत्तर—विद्याध्ययन एक तपश्चर्या है, जो विद्यार्थी को शुद्ध कर देती है—‘स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांङ्मयं तप उच्यते’ (गीता 17/15)।
मनुष्य जन्म का उद्देश्य है—परमात्मतत्त्व की प्राप्ति करना और उसका साधन है—संसार की सेवा। अतः लौकिक विद्या, धन, पद आदि का उपयोगी संसार की सेवा में ही है। ये संसार की सेवा में ही काम आ सकते हैं, परमात्मप्राप्ति में नहीं, क्योंकि परमात्मप्राप्ति लौकिक विद्या के अधीन नहीं है। जिसके पास लौकिक विद्या आदि है, उसी पर संसार की सेवा करने की जिम्मेवारी है। मालपर ही जकात लगती है और इन्कम पर ही टैक्स लगता है। माल नहीं है तो जकात कि बात की ? इन्कम नहीं तो टैक्स किस बात का ?
लौकिक विद्या, धन, पद आदि को लेकर संसार में मनुष्य की जो प्रशंसा होती है, वह एक तरह से मनुष्य की निन्दा ही है। तात्पर्य है कि महिमा तो लौकिक विद्या आदि की ही हुई, खुदकी तो निन्दा ही है। अतः जो लौकिक विद्या आदि से अपने को बड़ा मानता है, वह वास्तव में अपने को छोटा ही बनाता है।
प्रश्न—विद्याध्ययन बाल्यावस्थामें ही करना चाहिये या आजीवन ?
उत्तर—बाल्यावस्था में विद्याध्ययन करने का नियम केवल उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिये ही है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है,
उसको तो आजीवन शास्त्रों का, ब्रह्मविद्या का अध्ययन करते रहना चाहिये।
प्रश्न—अगर कोई विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हुए बीच में ही मर जाय तो उसकी क्या गति होगी ?
उत्तर—विद्याध्ययन एक तपश्चर्या है, जो विद्यार्थी को शुद्ध कर देती है—‘स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांङ्मयं तप उच्यते’ (गीता 17/15)।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book